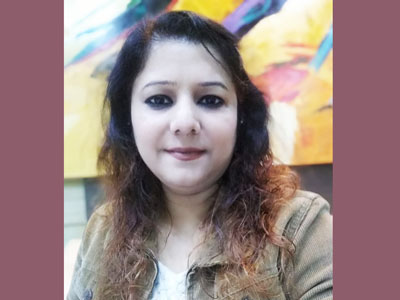मैं …
पहली बार मुझे
ज़िन्दगी मुश्किल लगी,
रोने वाली बात पर
मैं हँसने लगी,
हर छोटी बात
मुझे अखरने लगी,
दिल में शूल सी
चुभने लगी,
मेरी तर्कशीलता
आज़ादी और चंचलता
सभी को खटकने लगी,
मैं सबसे अलग दिखने लगी,
सिन्दूर,बिछिया, लाल चूड़ी
के चक्रव्यूह में फंसकर,
मैं अपने को कोसने लगी।
बेहतर थी,माता-पिता संग,
उनको भी देखती
और खुद को भी, समेटती थी,
लेकिन अब, पूरी तरह से
नहीं हो पाई,किसी की,
एक बेबस, लाचार
आश्रित, बेवकूफ सी
अपने ही पाँवों पर
मार कुल्हाड़ी,
मानो कैद
हो गई हूँ मैं।
छिन गई है आज़ादी,
वो बेबाकी से चीखना,
चिल्लाना, चहकना
वो हवा में उड़ना
पतंग सा लहराना,
वो आकाश छूने की
तमन्ना करना,
लेकिन अपने ही जख्मों पर
खुद नमक लगा
दिल हो गया है अब
इक टूटे खंडहर की तरह
जिसमें, ना कोई आता है
ना पास बुलाता है
ना देता है कोई आवाज़
ना रहता है अब कोई
मेरे दिल में,
अपनी खिलाफत
खामोशी से सुनती हुँ,
मैं इतना कह नहीं पाती
जितना महसूस करती हुँ।
चला गया वो मुझे छोड़
मैं रात भर रोती रही
जिंदगी के इस मोड़ को
अंधेरे में खोजती रही
उसे जाना था, वो चला गया
कभी ना लौटने के लिए
वो दगा मुझे दे गया
मस्ती सी मुझ संग कर गया
और मैं ठगी सी खुद में
दोष ढूँढती रह गई।
मेरा प्रेम ना तो हमउम्र था
ना हमख्याल
उम्र के फासले से
हरदम मैं डरती रही
एहसास मुझे रहता हरदम
उसके बड़े होने का
पिता, ससुर की भांति
बगल में खड़े होने का।
वो मेरे संग रहा, संग जुड़ा
पर साथी कभी नहीं बना
कभी विचार नहीं मिले
पर सदा साथ रहे
अधिकार कोई-कोई मिले
सत्कार कभी नहीं मिला
मैंने भी कभी
आवाज़ नहीं उठाई
पत्नी सदा रहती है छोटी
यही संस्कार थी
साथ में लाई।
© डॉ. प्रज्ञा शारदा, चंडीगढ़