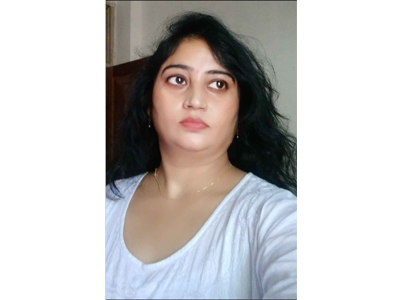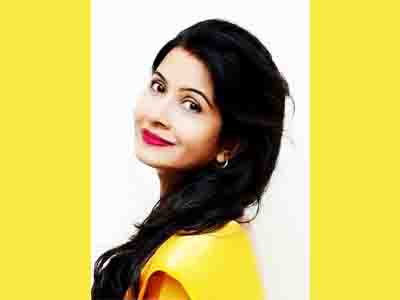मैं कौन हूं …
मैं कौन हूं? मैं क्या नहीं हूं? आत्मा क्या है? क्या मेरा है? क्या मेरा नहीं है? बंधन क्या है? मोक्ष क्या है? क्या भगवान हैं? भगवान क्या हैं? जगत कर्ता कौन है? क्या भगवान कर्ता हैं या नहीं? भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है? इस संसार के सच्चे कर्ता का स्वभाव क्या है? यह जगत कौन चलाता है? यह किस तरह से काम करता है? माया का सच्चा स्वरूप क्या है? जो कुछ भी हम जानते हैं, वह सच है या भ्रांति? जो कुछ भी ज्ञान हमारे पास है, उससे क्या हमारी मुक्ति होगी या बंधन ही रहेगा?
मित्रों, प्राय: आरम्भ से ही मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है, अज्ञात, अदृश्य, अनागत को जानने की उत्कृष्ट अभिलाषा, उनका विज्ञान समझने की प्रबल इच्छा आज मनुष्य को समय के उस दौर में लेकर आयी है जहाँ से उसके लिए समय और स्थान दोनों सिकुड़ चुके है, लेकिन मनुष्य के लिए उसके मूल प्रश्न, जो उसके अस्तित्व से सम्बंधित हैं, आज भी अनुत्तरित है और वो प्रश्न हैं- मैं कौन हूं? और क्यों हूं?
सज्जनों ! आज हभ जीव, ब्रह्म और प्रकृति के परस्पर सम्बन्धों और उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, चिदानंद स्वरुप ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त, सत, रज और तम गुणों वाली जो शक्ति होती है, प्रकृति कहलाती है, ये प्रकृति दो प्रकार की होती है, सत्व की शुद्धि से उस प्रकृति को माया और सत्व की अशुद्धि यानि मलिनता से उस प्रकृति को अविद्या कहा जाता है।
माया में पड़ा हुआ वो बिम्ब माया को अपने वश में रखता है, इस कारण से जीव सर्वज्ञ ईश्वर बन बैठा है, प्रकृति, मूलत: शक्ति होने के कारण स्वभावत: अस्थिर होती है, इसमें ब्रह्म का बिम्ब होने से ये ब्रह्म के नियंत्रण में रहती है, प्रकाशात्मक सत्व गुणों की शुद्धि से यानि जब वो सत्व गुण दूसरे गुणों से कलुषित नहीं हुआ होता तब वो प्रकृति माया कही जाती है।
जब वो सत्व गुण दूसरे गुणों से कलुषित होकर अशुद्ध हो जाता है तब वही प्रकृति अविद्या कहलाने लगती है, यानि कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है, कि विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को माया तथा मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहते हैं, माया में प्रतिबिम्बित उस आत्मा ने माया को अपने स्वाधीन कर रखा है और वही सर्वज्ञाता अनेक गुणों वाला ईश्वर हो गया है।
वही आत्मा रूपी ब्रह्म जब अविद्या में प्रतिबिम्बित होता है तो वो एक तरह से अविद्या के वश में फँस जाता है, वास्तव में अविद्या की विचित्रता के कारण वह एक से अनेक हो जाता है, इसी अविद्या को कारण शरीर कहते हैं, इस कारण शरीर कहलाने वाली अविद्या में अभिमान करने वाले को प्राज्ञ कहा जाता है, यहाँ अभिमान का अर्थ घमंड से नहीं लेना चाहिये, अभिमान का तात्पर्य यहाँ स्वयं के अनुभव करने से है।
अविद्या में प्रतिबिम्बित होकर उसके पराधीन हो जाने वाला आत्मा जीव कहलाने लगता है, वह जीव उस अविद्या रुपी उपाधि की विचित्रता के कारण अनेक प्रकार का हो जाता है, उसमें देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक भेद हो जाते हैं, इस अविद्या को कारण शरीर इसलिये कहा जाता है, क्योकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल और सूक्ष्म भूतों का कारण वही माना गया है, उस कारण शरीर में अभिमान करने वाले अथवा उसी में “मै” की भावना के वशीभूत जीव को प्राज्ञ कहा जाता है।
उन प्राज्ञों के भोग के लिए तम-प्रधान प्रकृति में से आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी नाम के पञ्च तत्व उत्पन्न हुयें, उन पञ्च तत्वों के अलग-अलग पांच सत्व भागों से क्रमानुसार- श्रोत्र (कान), त्वचा (स्पर्श), चक्षु (आँखें), रसना (जिव्हा) तथा घ्राण (नासिका) नाम की पांच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न हुयीं, अर्थात एक-एक तत्व के अलग-अलग सत्वांश से एक-एक ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति हुयीं, उन पाँचों तत्वों के पाँचों सत्वांशों को मिलाकर एक अंतःकरण नाम का द्रव्य (तत्व) उत्पन्न हुआ।
यह अंत:करण अपने वृत्तिभेद के कारण दो प्रकार का होता है, किसी की स्वाभाविक या चेष्टा को उसकी वृत्ति कहते हैं, जब यह अंत:करण, विमर्श अर्थात संशयात्मक यानि संशय से युक्त वृत्ति को मन कहते हैं, और जब यह निश्चयात्मक यानी निश्चयपूर्वक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, यही अंतर है मन और बुद्धि में, इसके बाद उन पाँचों तत्वों के अलग-अलग पाँचों रजों भागों से क्रमानुसार- वाक् (वाणी), हांथ, पैर, पायु तथा उपस्यथ यानी मल-मूत्र त्यागने के स्थान, ये पांच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुयीं।
अब जिस तरह से पाँचों तत्वों के सत्व भागों को मिलाकर अंत:करण उत्पन्न हुआ, उसी तरह से पाँचों तत्वों के रज भागों को मिलाकर एक प्राण की रचना हुई, ये प्राण अपने वृत्ति-भेद से अानि अपने काम के अनुसार पांच प्रकार का होता है- ये पांचों प्राण वायु रूप में भौतिक शरीर में उपस्थित होते हैं, ये पांचो प्राण हैं- प्राण, अपान, समान, उदान, तथा व्यान, इन पञ्च प्राणों का वर्णन आपको योग-प्राणायाम भगवद्गीता में पढ़ने को मिल जायेगा।
इस प्रकार से पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि इन सत्रह पदार्थों से मिलकर सूक्ष्म-शरीर बनता है, इसी को वेदान्तों में लिंग शरीर कहा गया है, या ब्रह्माण्डीय शरीर भी कहते, वह प्राज्ञ नाम का जीव उस लिंग शरीर में “मै” की भावना की वजह से, यानि की ये धारणा करना कि ये लिंग शरीर ही मैं हूं, ये ब्रह्मांडीय शरीर ही मेरा वास्तविक रूप है, तैजस हो जाता है, इसी प्रकार से जब ब्रह्म (आत्मा) यानि ईश्वर उस लिंग देह में “मै” की भावना करता है तो वह हिरण्यगर्भ हो जाता है।
इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि तैजस व्यष्टि है और हिरण्यगर्भ समष्टि इसके अतिरिक्त दोनों में कोई भेद नहीं, मलिन सत्व-प्रधान अविद्या रुपी उपाधि वाला जीव, जब लिंग शरीर में “मै” की भावना करता है तब वह उसी को अपनी आत्मा मानने लगता है, विशुद्ध सत्व-प्रधान प्रकृति को नियंत्रित करने की वजह से वो सर्व-व्यापी होता होता है, अत: वह समष्टि होता है, वह ईश्वर, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है, लिंग शरीर उपाधि वाले सभी तैजसों के साथ अपनी आत्मा की एकता को समझता है।
वो जानता है कि ये सब मिलकर मैं ही हूं, इसी वजह से वो समष्टि होता है, उस ब्रह्म से अन्य जो जीव हैं वो उस तादात्म्य के आभाव से, यानि उन सब के साथ एकत्व ज्ञान के न होने से व्यष्टि कहलाते हैं, ब्रह्म की इच्छा से प्रकृति, उन प्राज्ञ जीवों के भोग के लिए ही भोग्य यानी अन्न पान आदि, तथा भोगस्थानों- जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, और अंडज आदि प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति करने के लियें पञ्च तत्वों में से प्रत्येक तत्व को, पञ्चात्मक कर देती है जिससे कि उन जीवों के शरीर का निर्माण हो सके।