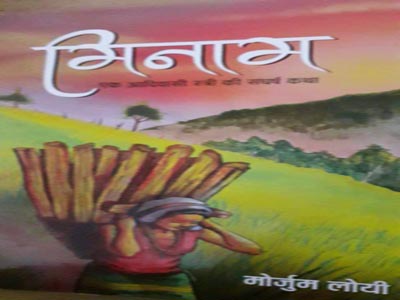अव्यक्त अनुभव ; आकाश …
सुनो,
क्यों गुमसुम से रहते हो?
इसीलिए न कि कोई समझता नहीं,
फिर तुम समझाते समझाते मौन हो गए हो,
प्रण कर लिया है न कि नहीं बोलोगे?
दिल के बंद दरवाजे को नहीं खोलोगे।
क्या मेरा अनुभव पर्याप्त नहीं?
सच तो ये है कि मैं तुम्हें सुनती हूं,
तुम्हारा विशाल अस्तित्व
जिसका न कोई आदि और अंत,
जैसे जंतर-मंतर भुलभुलैया।
तुममें खुद को खोती हूं,
मन के हाथों से तुम्हें छूती हूं,
पूरी की पूरी घुल जाती हूं।
उफ़!
बड़े चोर हो तुम।
पलक झपकते, जादू जैसे
गहरी रातों से नींद,
कत्थई आंखों से सपने,
और चुपके से मन को चुरा लेते हो।
हो जाती मैं निर्वाक, निर्बल और निश्चल,
अपने नीले, गहरे इंद्रधनुषी रंगों से,
भरकस सम्मोहित कर लेते हो।
कौन कहता है
कि तुम शुन्य हो,
शब्दों से, भावों से रिक्त
खालीपन हो..!
जरा कह दूं उन्हें
जैसे सागर अपने गर्भ में छिपाए
रत्न आभूषण,गरल- अमृत,
विनाश-जीवन और सभ्यताएं,
केवल करता है मौन गर्जना….
वैसे तुम भी तो छिपाए रहते हो
टिमटिमाते तारे,
मदमाता चांद, दपदपाता सूरज,
आकाशगंगा और जलती बूझती उल्काएं,
कितना कुछ है तुममें असीमित,
जिनसे मैं हूं सदा से अपरिचित।
सोचती हूं,
कोई कैसे अकेला हो सकता है….!
जब दिग्भ्रमित होकर
कोई थका हुआ पथिक,
तुम्हारी तरफ देखकर दिशा ढूंढ लेता है,
पा लेता है लक्ष्य को।
होगा कोई साथी विहीन पंछी,
कोई जीवन से हारा हुआ,
कोई दुःख, आह से भरा हुआ,
कहीं बैठा होगा और
सर उठाए देखता होगा तुम्हारी तरफ,
अचानक जब निकलता होगा मुख से
एक आह! या हे ईश्वर!
तब तुम ही बन जाते हो
उस एकान्त का साथी,
एक अप्रत्यक्ष देवता।
सुनो,
मैंने किया है महसूस तुम्हें…
गरजते हो तो डरते हैं सब,
पर मैं सुन लेती हूं उसमें छिपी ,
तुम्हारी सारी शिकायतें।
सावन में जब बारिश होती है,
तुम उदासी में रोते हो।
तुम्हारे आंसुओं से, उदासी से,
नहीं भीगी हूं केवल तन से,
बल्किभीगी हूं मन के पोर पोर से।
आकंठ पान किया है मीठे नमकीन आंसू को।
पर शुभ हो तुम, आशीष देते तुम्हारे अश्रु।
तभी नाचते हैं मोर, मनते हैं त्योहार,
लगती है मेहंदी, सजती है धरा,
सुखी होते हैं सब।
और तुम,
तुम रह जाते हो अव्यक्त वेदना से अभिषिक्त
और मैं अव्यक्त अनुभव से सिक्त….।