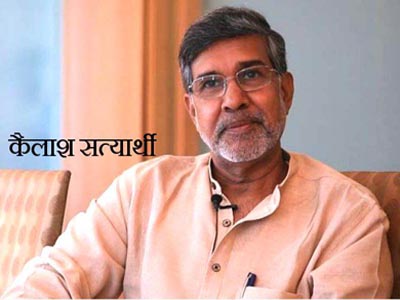मंज़रे-ए-ख़ाक …
हम जलता हुआ शहर और बाजार देखते रहे,
हम मंज़रे-ए-ख़ाक देखते रहे,
कहीं घर जला,
कहीं दुकान जली,
हम जलते हुए मकान देखते रहे,
हम जलता हुआ शहर और बाजार देखते रहे,
हम मंज़रे-ए-ख़ाक देखते रहे।
कहीं अमीर मरा,
कहीं गरीब मरा,
कहीं बूढ़ा मरा,
कहीं जवान मरा,
कहीं हिंदू मरा,
कहीं मुसलमान मरा,
हम इन आंखों से,
होता हुआ क़त्लेआम देखते रहे,
हम जलता हुआ शहर और बाजार देखते रहे,
हम मंज़रे-ए-ख़ाक देखते रहे।
कहीं किसी की हवेली जली,
किसी का घरौंदा जला,
किसी की झुग्गी जली,
किसी का सामान जला,
जला तो बस इंसान जला,
हम बेबस खड़े-खड़े,
आग का गुबार देखते रहे,
हम जलता हुआ शहर और बाजार देखते रहे,
हम मंज़रे-ए-ख़ाक देखते रहे।
कहीं गोलियां चली,
कहीं खंजर चले,
हम चाकुओं से होता हुआ क़त्लेआम देखते रहे,
खून किस – किस का गिरा? कौन मारा?
लाशों की होती हुई पहचान देखते रहे,
हम जलता हुआ शहर और बाजार देखते रहे,
हम मंज़रे-ए-ख़ाक देखते रहे।
कहीं स्कूल जले,
कहीं मंदिर जले,
कहीं मस्जिद जली,
जलाने वाले कौन थे? कहां से आए थे?
हम धर्म के ठेकेदारों से,
धर्म का होता हुआ अपमान देखते रहे,
हम मंज़रे-ए-ख़ाक देखते रहे।
दहशते खौफ में,
डरी सहमी औरतें,
रोती-बिलखती भागती,
अपने बच्चों को ढूंढती हुई,
तड़पती हुई मांओं को देखते रहे,
हम जलता हुआ शहर और बाजार देखते रहे,
हम मंज़रे-ए-ख़ाक देखते रहे।
©लक्ष्मी कल्याण डमाना, छतरपुर, नई दिल्ली